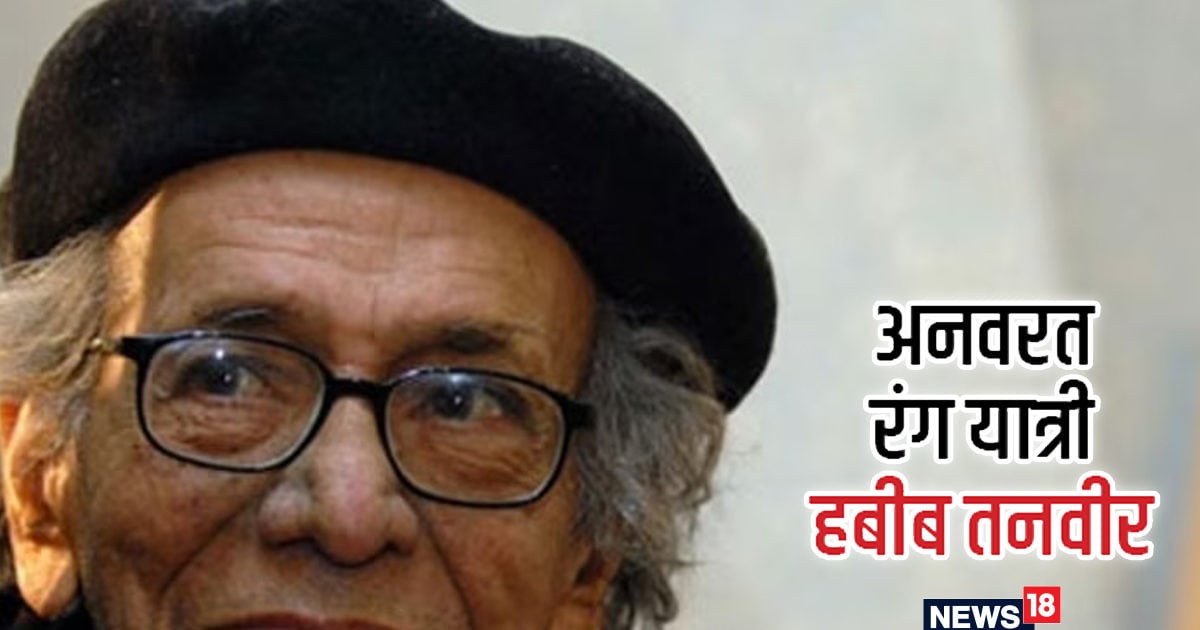(देवेंद्र राज अंकुर/ Devendra Raj Ankur)
भारतीय रंगमंच में ही नहीं, संपूर्ण विश्व रंगमंच में ऐसे किसी रंग-निर्देशक की मिसाल मिलना मुश्किल है, जिसने लगातार एक ही दिशा में, एक ही तरह का, एक ही नाट्य दल के साथ और अंततः एक ही अभिनेताओं के समूह के साथ लगभग साठ साल तक रंगकर्म किया हो.. ऐसे निर्देशक थे हबीब तनवीर. उन्होंने अपने दूसरे समकालीन निर्देशकों, यथा- उत्पल दत्त, शंभु मित्र और इब्राहिम अल्काजी के साथ-साथ ही अपने रंग-जीवन की शुरुआत की थी. लेकिन जहां बाकी दूसरे निर्देशक अपने अभिनेता, अपनी संस्थाएं और अपने कार्य की दिशाएं भी लगातार बदलते रहे, वहां हबीब तनवीर ने शुरू में ही जिस पगडंडी पर पैर रखा था, उसी पर चलते रहे. अपनी पीढ़ी के दूसरे निर्देशकों की तरह हबीब तनवीर की रंगयात्रा की शुरुआत भी पश्चिमी रंगमंच से साक्षात्कार और प्रशिक्षण के माध्यम से हुई.
साल 1969 में हबीब तनवीर की पहली प्रस्तुति देखने का अवसर मिला. प्रस्तुति थी ‘शतरंज के मोहरे’. प्रेमचंद की कहानी ‘शतरंज के खिलाड़ी’ पर आधारित होते हुए भी लगभग ढाई घंटे का संपूर्ण नाटक. हबीब तनवीर स्वयं भी एक मुख्य भूमिका में थे. प्रस्तुति की पूरी याद तो बाक़ी नहीं, हां, इतना जरूर है कि दो-तीन दृश्य-बंध परिवर्तनों के माध्यम से हबीब तनवीर ने एक विदेशी शासन व्यवस्था की पृष्ठभूमि में दो नवाबों की खिलाड़ियों से मोहरे होते जाने की परिणति को पकड़ने की कोशिश की थी. एक नया चरित्र मस्जिद में रहने वाला एक फकीर भी था, जो एक तरह का सूत्रधार या व्याख्याता भी कहा जा सकता है. यह भूमिका स्वयं हबीब तनवीर ने अभिनीत की थी. नाटक सीधे-सपाट संवादों के भीतर से उभरता था, उसमें किसी प्रकार के गीत-संगीत को प्रश्रय नहीं दिया गया था. पार्श्व संगीत था तो मात्र रिकार्डेड, जिसका प्रयोग संगीत की अपेक्षा ध्वनि प्रभाव के रूप में ज़्यादा किया गया था. प्रस्तुति से अधिक हबीब तनवीर का एक स्वतंत्र नाटककार, अभिनेता और निर्देशक का रूप एक जगह पर देखना मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी.
अगले ही वर्ष यानी 1970 में मुझे हबीब तनवीर के साथ काम करने का मौका मिला. ‘आगरा बाजार’ की पुनर्प्रस्तुति के पूर्वाभ्यास से लेकर उसके सत्रह प्रदर्शनों तक बतौर एक अभिनेता उनकी निर्देशकीय रचना-प्रक्रिया को भी निकट से जानने का अवसर मिला. ‘आगरा बाजार’ पहली बार 1954-55 में किया था हबीब तनवीर ने. तब से न जाने कितनी बार यह नाटक किया गया लेकिन यह अपने कथ्य और फार्म में आज भी उतना ही ताज़ा है. दरअसल, यह शुद्ध अर्थों में नाटक है ही नहीं. आगरा के मशहूर शायर नज़ीर अकबराबादी की 16 नज़्मों के माध्यम से तत्कालीन समसामयिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक वातावरण का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है.
प्रेम की असफलता ने ही मुझसे कहानियां लिखवाईं- ख्वाजा अहमद अब्बास
‘हयवदन’, ‘घासीराम कोतवाल’ या ‘जो कुमारस्वामी’ जैसे नाटकों से लगभग 15-20 बरस पहले ही ‘आगरा बाजार’ में लोक-तत्त्वों से भरपूर एक शैली को खोज लिया गया था. इस दृष्टि से ‘आगरा बाजार’ को हिंदी रंगमंच की पहली लोक-प्रस्तुति होने का श्रेय दिया जाना चाहिए. हबीब तनवीर ने यहां किसी प्रदेश विशेष की लोक-शैली का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि कथ्य की सामाजिकता में से वह शैली अपने आप ही उभरकर सामने आ गई. ककड़ी, पतंग, चूहा, बंदर, वेश्या, छैला- इन विविध विषयों पर लिखी गई नज़्मों ने स्वयं ही नाटक को लोक भूमि से जोड़ दिया. ‘आगरा बाजार’ अभिनेताओं के समूहन की दृष्टि से भी अद्भुत एनसाम्बल था – भटिंडा के दो फकीर मुख्य गायकों की भूमिका में, छत्तीसगढ़ के बहुत से लोक अभिनेता विविध भूमिकाओं में, विधिवत् प्रशिक्षित और अंततः शौकिया कलाकारों को भी मिलाकर की गई थी यह प्रस्तुति.
इसके बाद तो लगातार उनकी प्रस्तुतियां देखने को मिलीं. स्वयं उनसे भी अपने काम को लेकर सुनने का मौका मिला. इतनी सारी पृष्ठभूमि के भीतर से हबीब तनवीर के रंगकर्म को समझने की एक कोशिश सहज ही की जा सकती है, विशेषतः उनके नाटककार और निर्देशक वाले पक्ष पर केंद्रित करके.
उनके रंगकर्म की शुरुआत भले ही ‘हिंदुस्तानी थिएटर’ के साथ हुई, जहां पहली बार उनका परिचय अपने देश की संस्कृत नाट्य परंपरा और पश्चिम के ब्रेष्ट से हुआ लेकिन उनकी सही शुरुआत ‘नया थिएटर’ की स्थापना के साथ अपने लिखे नाटक ‘आगरा बाजार’ की प्रस्तुति के साथ होती है. पश्चिमी और भारतीय रंग-तत्त्वों के मेल से किस तरह का एक नया शिल्प और एक नया नाटक जन्म ले सकता है, उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ‘आगरा बाजार’. आगरा के मशहूर शायर नज़ीर अकबराबादी की नज़्मों और गज़लों पर आधारित यह नाटक न तो यथार्थवादी नाटक के त्रि-अंकीय शिल्प से कोई मेल खाता है और न ही लोक नाटकों के मनमोहक रंगों, गीतों, नृत्य एवं संगीत से भरपूर है. नाटक जिसकी शायरी पर आधारित वह तो कभी नाटक में आता ही नहीं, इसके साथ ही नाटक में भी कोई कहानी मौजूद नहीं है. इसके बावजूद यह नाटक नज़ीर अकबराबादी के समकालीन समाज, लोगों और रीति-रिवाज़ों की ऐसी दिलचस्प तस्वीर पेश करता है जो शायद ‘मृच्छकटिक’ और ‘अंधेर नगरी’ के बाद पहली बार देखने को मिलती है. इसीलिए इस तथ्य को कोरा संयोग कहकर नहीं छोड़ा जा सकता कि हबीब तनवीर ‘मृच्छकटिक’ अथवा ‘मिट्टी की गाड़ी’ की तरफ बार-बार लौटते रहते हैं. लेकिन आश्चर्य है कि जब पचास के दशक में हबीब तनवीर ने ‘आगरा बाजार’ की पहली बार प्रस्तुति की तो किसी ने उसका इस बात के लिए नोटिस नहीं लिया कि जिस भारतीय रंग-शैली की अपने देश को जरूरत थी. हबीब तनवीर ने इस नाटक के लेखन एवं प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उस वक्त तलाश कर ली थी, जब भारतीय रंगमंच में भारतीयता अथवा उसकी अपनी निजी पहचान, शैली और स्वरूप का डंका पीटने वाले नारों और मुहावरों का जन्म भी नहीं हुआ था- क्या यह एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है कि जिस दौर में भारतीय रंगमंच पश्चिम के तथाकथित यथार्थवादी प्रभाव में लेखन और प्रस्तुति के स्तर पर सक्रिय था, उसी क्षण हबीब तनवीर अपने नाट्यदल के साथ एक ऐसी रंग-शैली की तस्वीर पेश कर रहे थे, जो बाद में भारतीय रंगमंच में मील का पत्थर साबित हुई.
बहरहाल, हबीब तनवीर के रंगकर्म की तस्वीर कई प्रकार के दौरों और पड़ावों के भीतर से निकलकर अपना आकार ग्रहण करती है. हबीब की रंग-यात्रा के तीन पड़ाव हैं. पहले पड़ाव में ‘रुस्तम सोहराब’ और ‘मुद्राराक्षस’ जैसी प्रस्तुतियां हैं, जो पूरी तरह से शहरी और शौकिया अभिनेताओं के साथ की गईं. दूसरे पड़ाव में ‘आगरा बाजार’, ‘मिट्टी की गाड़ी’ जैसी प्रस्तुतियां हैं, जिनमें शहरी और लोक अभिनेताओं का संगम दिखाई पड़ता है और तीसरे एवं अंतिम पड़ाव में किया गया वह सब काम शामिल है, जो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के अभिनेताओं के साथ किया गया है. इसी दौर में ‘चरनदास चोर’, ‘बहादुर कलारिन’, ‘शाजापुर की शांतिबाई’ और ‘लाला शोहरत ‘राय’ जैसी प्रस्तुतियों के नाम लिए जा सकते हैं.
रंग-यात्रा की इस कड़ी को भाषा के प्रयोग की दृष्टि से भी पकड़ा जा सकता है. मूल अंग्रेजी, उर्दू या हिंदुस्तानी के साथ छत्तीसगढ़ी का इस्तेमाल और अंततः सिर्फ छत्तीसगढ़ी में ही लेखन और प्रस्तुतिकरण उन्हीं तीन पड़ावों से भी संबद्ध है. इप्टा, हिंदुस्तानी थिएटर से नया थिएटर तक लगभग छह दशकों की जो रंगयात्रा है, उसमें हबीब तनवीर की जितनी भारतीय दृष्टि समाहित है, उतनी ही वह पाश्चात्य दृष्टि भी, जो उन्हें पाश्चात्य रंगमंच के व्यावहारिक साक्षात्कार से प्राप्त हुई है. भले ही ब्रेष्ट के रंगमंच के व्यावहारिक अनुभव से पहले ही हबीब तनवीर ‘आगरा बाजार’ की रचना एवं प्रस्तुति कर चुके थे लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अगले नाटकों के लेखन में उन्हें ब्रेष्ट से बहुत मदद मिली.
एक निर्देशक के रूप में हबीब तनवीर ने संस्कृत नाटक, पारसी नाटक, ब्रेष्ट और मौलियर जैसे नाटककारों के नाटकों के अलावा या तो स्वयं ही नाट्य रूपांतर किए हैं अथवा मौलिक नाट्य-लेखन किया है. हबीब तनवीर ने अपने नाटकों के कथास्रोत मुख्यतः रंगमंच की मौखिक या ज्यादा से ज्यादा श्रव्य परंपरा में से ग्रहण किए हैं. प्रेमचंद की ‘शतरंज के खिलाड़ी’, नजीर की नज़्में, और ‘फितरती चोर’ भले ही प्रकाशित रूप में पहले से उपलब्ध रहे हों, लेकिन उनका बाकी नाट्यलेखन अपनी कहानी और गीतों के लिए लोक रंगमंच की मौखिक परंपरा पर निर्भर करता है. ‘राजा चंबा और चार भाई’, ‘बहादुर कलारिन’ या ‘रानी हिरमा की अमर कहानी’ आंचलिक क्षेत्रों, विशेषतः छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक-कथाओं, मिथक या रोजमर्रा के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई रचनाएं हैं. इस स्रोत का कोई लिखित रूप नहीं है. यहां तक कि ये स्रोत किसी भाषा-विशेष से उतने संबद्ध नहीं हैं, जितने कि बोली से- इसीलिए वे मौखिक परंपरा का हिस्सा है. स्वयं हबीब तनवीर के अभिनेता भी लोक रंगमंच की इसी परंपरा का हिस्सा है.
हबीब तनवीर का रंगकर्म एक और मायने में भी रेखांकित किया जा सकता है. उन्होंने कभी भी अपने रंगकर्म को एक दर्शन, एक विचारधारा अथवा किसी सिद्धांत का जामा पहनाने की कोशिश नहीं की. कभी उनसे गोष्ठियों और सेमिनारों में यह सवाल किया भी गया कि आप इस प्रकार का रंगकर्म क्यों करते हैं तो उनका सीधा-सा जवाब यही रहा है कि मैं ये सब मजे के लिए करता रहा हूं. लोगों को हमेशा इस उत्तर से बेहद निराशा हुई है, क्योंकि उनके लिए यह कल्पना करना बेहद मुश्किल हो जाता है कि महज मजे के लिए ही कोई रंग-निर्देशक अपनी जिंदगी की आधी सदी गुज़ार दे. लेकिन ये तथाकथित बुद्धिजीवी जब हबीब तनवीर के इस स्पष्टीकरण पर झल्लाते नजर आते हैं तो वे इस सत्य और तथ्य को शायद बिलकुल भूले हुए होते हैं कि आज से लगभग दो-ढाई हजार वर्ष पहले भरत ने भी रंगकर्म के माध्यम से ऐसा ही मजा अथवा सुसंस्कृत शब्दावली में कहें तो ‘आनंद’ या लोकानुरंजन करने की बात नहीं की थी?
भरत और उनके ‘नाट्यशास्त्र’ को एक मिथक मानकर कुछ देर के लिए छोड़ भी दिया जाए तो बीसवीं शताब्दी के सबसे बड़े रंग-चिंतक एवं निर्देशक नाटककार ब्रेष्ट ने भी अपने नाटकों और रंगकर्म का उद्देश्य यही माना है- पहले मनोरंजन और फिर उस के माध्यम से शिक्षा देने का काम.
रंग-व्यक्तित्व की दृष्टि से हबीब तनवीर का कौन-सा पक्ष ज्यादा दिनों तक याद रखा जाएगा? इसमें कोई संदेह नहीं कि उनका अभिनेता और निर्देशक वाला पक्ष अधिक मुखर होकर सामने आता है. लेकिन सच्चाई यही है कि उनका नाटककार ही सबसे ज्यादा ठोस और सार्थक है. हर बार किसी जाने-पहचाने नाटक की बजाय बिलकुल नए नाटक की रचना उनकी ऊर्जा का परिचायक है. सिर्फ नया नाटक ही नहीं, हर बार उस नए नाटक के लिए एक नई बुनावट तैयार करना हबीब तनवीर की ताज़गी को रचना के स्तर पर सूचित करता रहा. अपनी प्रस्तुतियों में हबीब तनवीर भले ही दोहराव के शिकार हों, लेकिन उनके नाटक अपने कथ्य एवं फॉर्म में एक-दूसरे से बिलकुल अलग हैं. इतना ही नहीं, ये नाटक अपने ढाँचे में बेशक लोक-शैली का अनुसरण करते हों लेकिन कथ्य की दृष्टि से बिलकुल आधुनिक, समसामयिक और यहां तक कि आश्चर्यजनक रूप से मौलिक भी जान पड़ते हैं.
हबीब तनवीर ने अपनी लगभग साठ वर्षों की अनवरत रंग यात्रा में भारतीय रंगमंच को जो कुछ दिया है, उसका ऐतिहासिक महत्त्व कभी कम नहीं होगा और यह महत्त्व कम-से-कम तीन दिशाओं में अवश्य दिखाई पड़ता है- ‘आगरा बाज़ार’ जैसे नाटक की रचना ने भारतीय नाट्य लेखन के सामने वह आदर्श प्रस्तुत किया कि किस प्रकार यथार्थवादी ढाँचे से अलग होकर भी पूर्व और पश्चिम की नाट्य परंपराओं के मेल से एक नए फिल्म के शिल्प के साथ नाट्य रचना की जा सकती है, जिसमें लोक नाट्य शैलियों की कोई जबर्दस्ती से इकट्ठी की हुई खिचड़ी नहीं मिलाई गई है. फिर भी उसमें अपने स्वयं के लोकरंग की झलक दिखाई पड़ती है. ‘मिट्टी की गाड़ी’ ने संस्कृत नाटकों के मंचन का वह सहज और सरल रास्ता सुझाया जो ठेठ हिंदुस्तानी लोकधर्मी यथार्थवादी होते हुए भी निहायत ही सांकेतिक एवं अमूर्त जान पड़ता है और संस्कृत नाटकों में उपलब्ध समय, स्थान और कार्य-व्यापार की उन्मुक्तता की समस्याओं को सुलझा लेता है. ‘चरनदास चोर’ की प्रस्तुति शुद्ध रूप से एक लोककथा को कैसे आधुनिक एवं समकालीन बनाया जाए भारतीय रंगमंच में इस खोज का सर्वश्रेष्ठ विकल्प है.
ये सारे निष्कर्ष हबीब तनवीर द्वारा लगातार खोजी एवं व्यवहार में लाई जाने वाली भारतीय रंगशैली के साक्ष्य के रूप में सदैव याद किए जाते रहेंगे और भावी रंगकर्मियों के लिए पथ-प्रदर्शन का काम करेंगे.
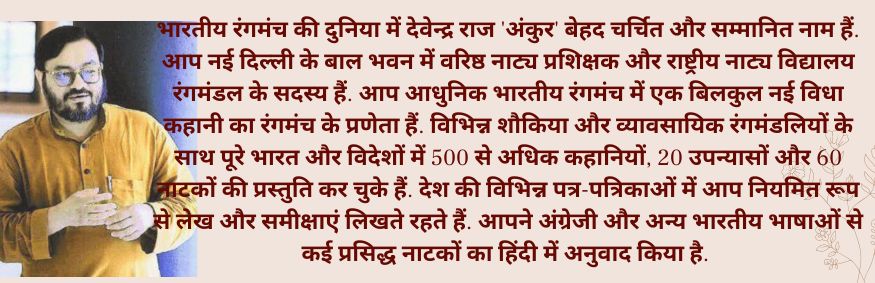
.
Tags: Literature, Literature and Art
FIRST PUBLISHED : June 08, 2023, 07:00 IST